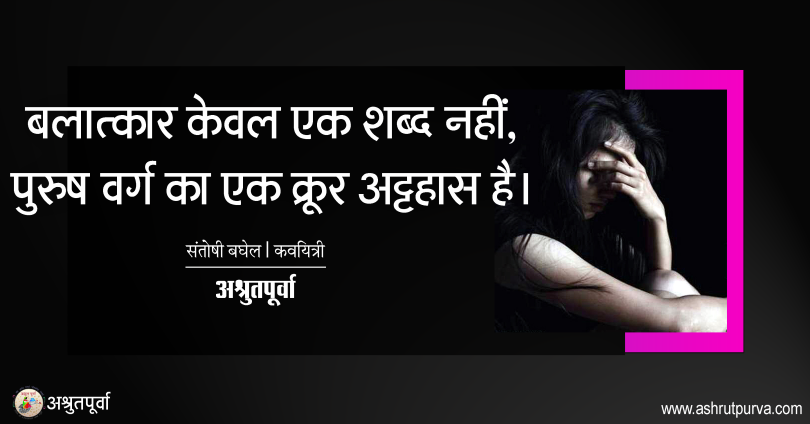संतोषी बघेल II
अकसर शब्द मायने खो देते हैं,
बन जाते हैं रूढ़,
जिन दिनों मैंने बस पढ़ना शुरू किया था
या शायद थोड़ी समझदार हुई थी
ठीक उन्हीं दिनों पहले-पहल
बलात्कार शब्द गूंजा था जेहन में,
कौतूहल हुई थी, पर उन दिनों
नहीं था इतना खुलापन,
न आज सा सबकुछ उपलब्ध था कहीं!
किसी से पूछने का अर्थ था झिड़कियां खाना,
और तब इतना साहस भी कहां था मुझमें!
बस इसमें ‘अमुक पीड़िता’ पढ़ कर
कहीं मन सब समझने लगा था,
और साथ ही एक भय भी
उगता जा रहा था मेरे अंदर…।
उस भय को पोषित करने में
समाज ने कितनी महती भूमिका निभाई थी!
वर्जित विषयों की तरह होते थे
तब ये बलात्कार जैसे शब्द…।
और उन्हीं विषमताओं में हमने
अपना किशोरवय जिया था…।
रच बस गई हैं उन दिनों की
विषमताएं मुझमें और आज भी
वो डर मुझमें सांसें ले रहा है!
ये शब्द जब जिस रूप में मेरे समक्ष आता है,
मैं कांप जाती हूं
ताश के पत्तों की तरह
मेरा साहस ढह जाता है…।
ये शब्द केवल शब्द नहीं हंै,
एक क्रूर अट्टहास है समूचे पुरुष वर्ग का!
स्त्रीत्व के मखौल के लिए इससे
वीभत्स शब्द हो ही नहीं सकता था!
इस शब्द को कोई विस्मृत
भी कैसे कर सकता है?
स्त्री की अस्मिता के ठीक विपरीत
इसने खुद को आरूढ़ किया है,
कह सकते हैं ये स्त्री की
अस्मिता का ही बलात्कार है
और ये तब तक रुढ़ रहेगा
जब तक स्त्री केवल देह रहेगी…।
शेष तब तक लोग बलात्कार के कारणों पर,
चर्चा परिचर्चा में रमे रहें और
कहीं न कहीं कारण स्वयं स्त्री को मान
अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर दें…।
यही तो होता आया है न?